दक्षिण मेरु : बृहदेश्वर मंदिर
भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति, इतिहास और असाधारण वास्तुकला सदियों से संरक्षित मंदिर की दीवारों पर दिखाई देती है। हिंदू धर्म के उदय के साथ, भारत विभिन्न देवी-देवताओं को समर्पित कई मंदिरों की स्थापना का साक्षी बना। अपने आप में अद्वितीय, देश भर में फैले मंदिरों को उनके क्षेत्र, वास्तुशिल्पीय शैली और जटिलता के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया।
शिल्पशास्त्र के अनुसार, भारत के मंदिरों को तीन प्रकार की शैलियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- नागर शैली (उत्तर भारतीय शैली), ये मंदिर हिमालय और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच की भूमि से संबंधित हैं।
- द्रविड़ शैली (दक्षिण भारतीय शैली) ये मंदिर कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच की भूमि से संबंधित हैं।
- वेसर शैली (उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का मिश्रण) ये मंदिर विंध्य पर्वतमाला और कृष्णा नदी के बीच की भूमि से संबंधित हैं।

नागर शैली के मंदिर का शिखर

द्रविड़ शैली के मंदिर का विमान
द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताएँ जो उसे अन्य दो शैलियों से अलग करती हैं:
विमान - विमान गर्भगृह के ऊपर बनी ऊँची संरचना होती है। यह संरचना एक पिरामिड जैसी होती है और इसकी योजना वर्गाकार होती है। इसमें कई मंजिलें होती हैं जो आकार में घटती हुईं एक के ऊपर एक बनाई जाती हैं।
स्तूपिका - स्तूपिका एक बड़ा पत्थर है जो विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर स्थित होता है। स्तूपिका के ऊपर कलश होता है, जिसके कारण विमान की ऊँचाई और अधिक बढ़ जाती है।
गोपुरम - गोपुरम मंदिर के बड़े प्रवेश द्वार को कहते हैं, जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली की ख़ास विशेषता है। गोपुरम का विकस समय के साथ हुआ है और यह दक्षिण भारत के बाद के मंदिरों का केंद्र बिंदु बन गया है। बाद के मंदिरों में ऊँचे गोपुरम हैं, जो अक्सर विमान से भी ज़्यादा ऊँचे होते हैं।

विशिष्ट द्रविड़ शैली में बना एक गोपुरम या प्रवेश द्वार
द्रविड़ शैली के मंदिरों के कुछ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में हैं। इनमें से एक चोल साम्राज्य के शक्तिशाली राजा, राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, जो अपनी भव्यता और असाधारण स्थापत्य विशेषताओं के लिए जाना जाता है।
तंजावुर की स्थापना मुथरैयार राजाओं द्वारा की गई थी और यह शहर उनकी राजधानी थी। तंजावुर नाम की उत्पत्ति के विभिन्न संस्करण हैं। एक संस्करण के अनुसार इसका नाम तंजन नामक असुर के नाम से लिया गया है। यह मान्यता है कि तंजन ने आस-पास के क्षेत्रो में अराजकता फैलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप श्री आनंदवल्ली अम्मन और श्री नीलमेघपेरुमल (विष्णु) को उसे नष्ट करना पड़ा, लेकिन ऐसा करने से पहले भगवान विष्णु ने, उसके नाम पर शहर का नाम रखने की उसकी अंतिम इच्छा को स्वीकार लिया था। दूसरे संस्करणों के अनुसार शहर का नाम ‘तंजम’ शब्द से लिया गया है जिसका तमिल भाषा में अर्थ ‘शरण’ होता है। इसलिए तंजावुर का अर्थ 'शरण का शहर' है।
तंजावुर पर चोलों से लेकर नायकों, मराठों और अंत में अंग्रेज़ों तक का शासन रहा। इन सभी में, चोल राजवंश को ही आधुनिक तंजावुर का निर्माता माना जाता है।
चोलों ने मुख्य रूप से तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र पर शासन किया। हालाँकि ऐसा लगता है कि वे संगम काल से ही सत्ता में थे,परंतु उन्हें नौवीं शताब्दी में प्रख्याति मिली और तेरहवीं शताब्दी तक वे शासन करते रहे। चोल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक, विजयालय, ने एक छोटे से राज्य की स्थापना की थी और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तंजावुर राजराजेंद्र चोल के शासनकाल तक चोलों की राजधानी रही, जिन्होंने फिर राजधानी को गंगाईकोंडाचोलापुरम में स्थानांतरित कर दिया। चोल राजाओं, राजराज प्रथम (985 ईस्वी – 1012 ईस्वी) और उनके बेटे राजराजेंद्र को उनकी नौसेना और सैन्य ताकत और दक्षिण भारत की सीमाओं के आगे भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जाना जाता है।

चोल साम्राज्य को दर्शाता हुआ नक्शा

राजराज चोल प्रथम की मूर्ति
चोल शासक भगवान शिव के उपासक थे। चोलों द्वारा बनाए गए सबसे शुरुआती मंदिरों में से एक चिदंबरम का नटराज मंदिर है। 985 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठने वाले राजराज प्रथम ने वर्ष 1004 ईस्वी में चिदंबरम के मंदिर को कई बड़े अनुदान और उपहार दिए। कृतज्ञतावश, मंदिर के अधिकारियों ने उन्हें 'श्री राजराज' और 'शिवपदशेखर' की उपाधियाँ प्रदान कीं। कुछ लोगों का मानना है कि इसी समय, उन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर में, भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर की स्थापना पर विचार किया। दूसरे लोगों की राय है कि राजराज द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद, उन्हें 'सम्राटों में शेर' के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए भगवान शिव को समर्पित इस भव्य मंदिर का निर्माण किया।

तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर की योजना की चित्रलिपि
राजराज प्रथम ने अपने शासनकाल के उन्नीसवें वर्ष में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। इस इमारत और उसके निर्माण से संबंधित जानकारी का एक प्रमुख स्रोत वे शिलालेख हैं जो मंदिर के चबूतरे पर चारों ओर मौजूद हैं। एक शिलालेख में लिखा है, 'राजा ने अपने शासनकाल के पच्चीसवें वर्ष (1010 ई.) के दो सौ पचहत्तरवें दिन पर, मंदिर के विमान के शीर्ष पर लगाए जाने वाले सोने के कलश को उपहार के रूप मे दिया है'। इसका अर्थ यह है कि इस वास्तुशिल्पीय रूप से भव्य मंदिर को पूरा करने में केवल छह वर्ष लगे थे।

आज बृहदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध, राजराजेश्वरम मंदिर
राजराज ने अपने नाम पर इस मंदिर का नाम राजराजेश्वरम रखा था। राजा ने मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया और शिलालेखों के अनुसार यह लिंग ‘आडवालन’, ‘दक्षिण मेरु विटंकण’ और ‘राजराजेशवरम उडैयार’ नामों से जाना गया। मंदिर परिसर में अम्मन मंदिर का निर्माण करने वाले पंड्यों के शासनकाल के दौरान भी, यह मंदिर इसके निर्माता द्वारा दिए गए नाम से जाना जाता रहा। ऐसा कहा जाता है कि वर्षों बाद, इस मंदिर के देवता का नाम ‘तिरु पेरुवुडैयार (तमिल में महान भगवान) पड़ा, जिसका संस्कृत में ‘बृहत्-ईश्वर’ के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। अम्मन को संस्कृत नाम, ‘बृहत् नायकी’ या ‘बृहण नायकी’ (महान महिला) दिया गया। यह मंदिर को दिए गए ‘बृहदेश्वर ' नाम का मूल हो सकता है, हालाँकि उस समय के किसी भी शिलालेख या भजन में इस मंदिर का नाम ‘राजराजेश्वरम’ से ‘बृहदेश्वर’ में बदल दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
कावेरी के तट के पास स्थित, बृहदेश्वर मंदिर चोलों की तत्कालीन राजधानी तंजावुर की सबसे ऊँची संरचना है। क्षेत्र में उच्चतम बिंदु पर खड़े, इस वास्तुशिल्पीय अविष्कार को गारे या किसी अन्य चिपकने वाले पदार्थ के उपयोग के बिना निर्मित किया गया था। शिलालेखों में अभिलिखित है कि शासक द्वारा परिकल्पित योजना को निष्पादित करने वाले मुख्य वास्तुकार का नाम राज राज पेरुन्थचन (‘पेरुम’ अर्थात ‘बड़ा’ और ‘थचन’ अर्थात ‘बढ़ई’) था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस समय के कुछ महानतम मंदिरों का निर्माण किया था, जिससे पता चलता है कि राजराज ने इस महान मंदिर को बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों, कारीगरों और मूर्तिकारों को नियुक्त किया था।
इस मंदिर के बारे में एक में आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके निर्माण के लिए, स्थानीय रूप से अनुपलब्ध, ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के लिए दूर के इलाकों से अच्छा ग्रेनाइट लाया गया था। हालाँकि यह कहाँ से लाया गया था, इसकी सही जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि तंजावुर से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित मम्मलाई नामक एक पहाड़ी से इसका उत्खनन किया जाता था।

मंदिर के चबूतरे के चारों ओर उत्कीर्णित शिलालेख
राजा ने इसके निर्माण के लिए कई अनुदान दिए। यह मंदिर राजराज की अद्भुत उपलब्धियों का प्रतिबिंब भी है। ऐसा कहा जाता है कि चालुक्य राजा, सत्यश्रय, को पराजित करने के बाद उन्होंने जिस विशाल खज़ाने पर कब्ज़ा कर लिया था, उसका उपयोग इस मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया गया था। मंदिर के शिलालेखों में राजा की रानियों, उनकी बहन कुंडवई, सरदारों और अन्य अधिकारियों द्वारा मंदिर को दिए जाने वाले अलंकृत उपहारों के विस्तृत वर्णन हैं। इसकी सुंदरता से कोई समझौता किए बिना, इस तरह की शानदार संरचना का निर्माण करने के लिए कई यात्रियों और उस समय के अन्य आगंतुकों ने राजराज और उनके वास्तुकारों की प्रशंसा की थी।
मंदिर और इसके घटक पूर्व पश्चिम अक्ष पर स्थित हैं। बृहदेश्वर मंदिर की योजना में एक गर्भगृह शामिल है, जिसके ऊपर विमान बना है और जो अर्धमंडप के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद महामंडप, मुखमंडप और नंदी मंदिर हैं। मंदिर प्रांगण मे, भगवान गणेश, सुब्रह्मण्यम, देवी बृहन्नायकी, चंडिकेश्वर और भगवान नटराज को समर्पित मंदिर भी हैं। यहाँ अष्ट दिकपाल को समर्पित मंदिरों के प्रमाण भी उपस्थित हैं, जिनमें से अब केवल कुछ ही बचे हैं।

बृहदेश्वर मंदिर की योजना
एक दोहरी दीवार वाले प्रांगण के भीतर स्थित, बृहदेश्वर एक विशिष्ट द्रविड़ शैली का मंदिर है जिसमें प्रवेश करने के लिए पूर्व में बड़े प्रवेश द्वार हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। इस मंदिर में विशेष रूप से दो गोपुरम हैं, जिनमें से पहला केरलंतकन गोपुरम है जिसे राजराज की चेरों पर जीत हासिल करने पर बनाया गया था। इस गोपुरम में पाँच मंजिलें हैं और दूसरे गोपुरम की तुलना में यह कम अलंकृत है। कुछ मीटर की दूरी पर, मंदिर के चारों ओर बनी दीवार (कृष्णन रमन तिरुच-चुरू-मलिगई) को भेदता हुआ, दूसरा गोपुरम है, जिसे राजराजन गोपुरम कहा जाता है। यह गोपुरम पुराणों के दृश्यों के साथ विस्तृत रूप से सजाया गया है और इसमें प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले, पत्थर के एक-एक खंड से बने दो द्वारपाल हैं। इस गोपुरम में भगवान शिव के जीवन के दृश्यों की नक्काशी भी है।

बृहदेश्वर मंदिर के दो गोपुरम (प्रवेश द्वार)

नंदी मंडप के अंदर स्थित, पत्थर के एक खंड से बनी नंदी की प्रतिमा
गोपुरम के आगे नंदी मंडप है, जो मंदिर में बाद में जोड़ा गया था। नायक शासकों द्वारा निर्मित, इस मंडप में पत्थर के एक खंड से बनी विशाल नंदी की प्रतिमा (भगवान शिव का वाहन) है, जो लगभग 12 फ़ीट ऊँची और 8 फ़ीट चौड़ी है। नंदी मंडप की छत को नायक शासकों की सुंदर चित्रकारियों से सजाया गया है।
नंदी मंडप के बाद मुखमंडप और महामंडप हैं। मुखमंडप में प्रवेश करने के लिए सीढ़ीयाँ बनी हैं। मुखमंडप में भैरव की मूर्ती है, और यह मंदिर परिसर के अष्ट परिवार मंदिरों का एक भाग रहा होगा। इस संरचना के आगे स्तंभों वाला सभागृह है जिसे महामंडप कहा जाता है।
इसके आगे अर्धमंडप है जो गर्भगृह से जुड़ा हुआ है। इस संरचना में सामने और उत्तरी और दक्षिणी ओर पर बने विशाल प्रवेश द्वारों के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है। एक ऊँचे चबूतरे पर स्थित और अपने दोनों ओर बने द्वारपालों सहित, अर्धमंडप के प्रवेश द्वार तक सीढ़ियों से चढ़ा जा सकता है। इस मंडप के केंद्र में स्थित स्नान मंच के कारण इसको देवता का स्नान कक्ष कहा जाता है।

ऊँचे विमान सहित गर्भगृह का चित्र
इसके आगे, दो मंज़िला गर्भगृह है जिसके केंद्र में एक विशाल लिंग स्थित है। दो मंज़िलों जितना बड़ा, यह शिव लिंग, उस समय के सबसे विशाल लिंगों में से एक माना जाता है। गर्भगृह एक ऊँचे चबूतरे पर स्थित है और इसकी योजना वर्गाकार है। इसके चारों ओर एक गलियारा है जो संभवतः परिक्रमा पथ है। जहाँ इस गलियारे की पहली मंज़िल की दीवारें अपने समय के सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्रों से सजी हैं, वहीं दूसरी मंज़िल में करण मूर्तियाँ हैं, जो शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम का आधार हैं। यह गर्भगृह एक ऐसा स्थान है जहाँ कला के विभिन्न पहलू एकजुट होकर चोलों की कलात्मक उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं।
कला के सबसे खूबसूरत और असाधारण कार्यों को दर्शाता, मंदिर का यह गलियारा तब तक बंद पड़ा रहा, जब तक अन्नामलाई विश्वविद्यालय के प्रो. एस. के. गोविंदस्वामी ने मंदिर का दौरा करने का फैसला नहीं किया था। उन्होंने अपनी छोटी पेट्रोमैक्स लालटेन का उपयोग करते हुए, वहाँ सत्रहवीं शताब्दी के नायक शासकों के काल की चित्रकारियाँ खोज निकाली। चोल चित्रकारियों को खोजने की आशा में उन्होंने अपने प्रयत्न जारी रखे। जल्द ही, उन्होंने एक ऐसा भाग खोज निकाला जिसमें नायक चित्रकारियों का ऊपर का पलस्तर उतर रहा था।

राजराज चोल प्रथम को उनके गुरु, करुवुर देवर के साथ दर्शाती एक चोल चित्रकारी

नृत्य करती लड़कियों को चित्रित करता हुआ भित्ति चित्र
दीवार की ऊपूरी सतह पर बनी नायक चित्रकारियों और उसके नीचे चोलों द्वारा बनाई गईं मूल चित्रकारियों, दोनों सतहों के संरक्षण के प्रयास किए गए।
चोल भित्ति चित्रों को बनाने से पहले, चूने के पलस्तर का उपयोग करके सतह को तैयार किया गया था। खुरदरी पत्थर की दीवार पर इस पलस्तर की दो परतें लेपित की गईं थीं, जिसपर पलस्तर के गीला रहते चित्रकारी बना दी गई थी। लैपिस लज़ूली से प्राप्त नीले रंग को छोड़कर, इन चित्रकारियों में उपयुक्त बाकी सभी रंग प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए गए थे।
कला की असाधारण रचनाओं में से एक शिव की त्रिपुरांतक के रूप में चित्रकारी है। त्रिपुरांतक को एक रथ की सवारी करते हुए दर्शाया गया है, जिसे भगवान ब्रह्मा द्वारा चलाया जा रहा है। साथ में भगवान शिव के दो पुत्र, गणेश और कार्तिकेय अपने-अपने वाहन क्रमशः मूषक और मोर और देवी काली अपने शेर पर सवार हैं, और सामने नंदी भी हैं। त्रिपुरांतक को आठों हाथों में हथियार के साथ दिखाया गया है, जो असुरों से लड़ने के लिए तैयार हैं, जिनकी आँखें क्रोध से भरी हुई हैं फिर भी उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान है। यह चित्रकारी अपने उग्र विषय और कैसे उस समय के कलाकार इन पात्रों की वास्तविक अभिव्यक्तियों को सामने लाने में सफल रहे, के लिए जानी जाती है।
गलियारे की अन्य प्रसिद्ध चित्रकारियों में एक नटराज की है जिसमें उन्हें राजराज प्रथम और उनकी रानियों द्वारा पूजा जा रहा है। चित्रकारी में नटराज को चिदंबरम मंदिर की चित सभा में दिखाया गया है। रानियों द्वारा पहनी गईं विभिन्न डिज़ाइनों की साड़ियों का चित्रण इस चित्रकारी का विशेष तत्व है।
गर्भगृह का ऊपरी मंज़िल का गलियारा नृत्य की आकृतियों से सुसज्जित है जिसमें शिव के करणों का चित्रण किया गया है, जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में है। ये मूर्तियाँ 108 करणों में से 81 करणों को दर्शाती हैं, जबकि पत्थर के अन्य खंडों को खाली छोड़ दिया गया है।

दक्षिणा मेरु के नाम से भी प्रसिद्ध, विशाल विमान
गर्भगृह के ऊपर बना हुआ विमान बृहदेश्वर मंदिर की सबसे खास विशेषता है। तेरह मंज़िलों के साथ 200 फ़ीट ऊँचे इस विशालकाय विमान को भगवान शिव के आवास कैलाश पर्वत के नाम पर दक्षिणा मेरु कहा जाता है। आकार में कम होती जाती कई मंज़िलों सहित, यह संरचना पिरामिड जैसी प्रतीत होती है। वास्तु शास्त्रों के अनुसार, पाँच से अधिक मंज़िलों के विमान (जिसे मुख्य विमान कहा जाता है) को श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे ऊँचे विमानों में से एक से युक्त, बृहदेश्वर मंदिर शासक की शक्ति और क्षेत्र पर उसका प्रभुत्व दर्शाता है।
विमान को अन्तःपाशी (इंटरलॉकिंग) तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है जिसमें पत्थर के खंडों को विशेष रूप से रखा जाता है, जिसके कारण पूरे ढाँचे पर समान रूप से दबाव वितरित होता है। विमान का आधार, उसके ऊपर बनी विशाल संरचना का भार उठाने के लिए पर्याप्त रूप से चौड़ा है। परिणामस्वरूप विमान, बिना किसी झुकाव के, सीधा खड़ा हुआ है।
पूरा विमान सुंदर रूप से सजाया गया है, जिसमें प्रत्येक मंजिल में नियमित अंतराल पर आले और देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुईं हैं। विमान का मुख्य आकर्षण स्तूपिका (अंतिम मंजिल के ऊपर बनी एक बड़ी गुंबददार संरचना) है।
वर्षों से, इंजीनियरों और वास्तुकारों ने यह समझने की कोशिश की है कि 80 टन से अधिक वजन के पत्थर के एक खंड से बनी इस स्तूपिका को इतनी ऊँचाई तक कैसे उठाया गया होगा। यह माना जाता है कि एक रैंप, या एक ढलान वाला पथ बनाया गया था और लगभग एक हजार बंदी हाथियों ने इस पत्थर को विमान के शीर्ष तक पहुँचाया था। इतनी ऊँचाई तक पहुँचने के लिए रैंप चार मील लंबा था और इसे, पास में स्थित सारपाल्लम नामक गाँव से शुरू किया गया था।
स्तूपिका के दोनों कोनों में दो नंदी की आकृतियाँ हैं, जो मुड़कर बैठी हैं परंतु उनके सिर सामने की ओर हैं। स्तूपिका के ऊपर सोने से ढका कलश है जिसका उल्लेख शिलालेखों में किया गया है और यह मंदिर की अंतिम संरचना है।

बैठे हुए नंदी के साथ सजाया पत्थर का 80 टन का खंड (स्तूपिका)

चंडिकेश्वर मंदिर
मंदिर परिसर के भीतर अन्य छोटे मंदिरों में सुब्रमण्यर और गणेश मंदिर हैं जो शायद अष्ट परिवार देवता का भाग थे। इनमें से एक, संत और मुख्य प्रशासक, चंडिकेश्वर को समर्पित मंदिर, एकमात्र ऐसा मंदिर है, जो राजराज द्वारा परिकल्पित मूल योजना का हिस्सा था और अपने मूल स्वरूप में आज भी मौजूद है। विमान के निकट स्थित, यह एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें राजराज द्वारा दर्ज, कुछ शुरुआती शिलालेख हैं।
समय के साथ, मंदिर के परिसर में कई अतिरिक्त संरचनाएँ जोड़ी गईं। राजराज द्वारा परिकल्पित यह वास्तुशिल्पीय अचंभा ऐसा था कि मंदिर परिसर में बाद में बनाई गईं किसी भी अतिरिक्त संरचनाओं के कारण मूल योजना में कोई बदलाव नहीं आया। समय के साथ, मंदिर परिसर में कई छोटे मंदिरों और मंडपों को जोड़ा गया है, जैसे कि भगवान नटराज का मंदिर और अम्मन या बृहन्नायकी को समर्पित मंदिर।
बृहदेश्वर मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा केंद्र भी था जहाँ लोग बड़ी संख्या में शाम को इकट्ठा होते थे, और संगीतकारों के गायन के साथ देवदासियों का नृत्य देखा करते थे। शिलालेखों के अनुसार इस भव्य मंदिर को रोशन करने के लिए लगभग 160 दीपक और मशालें जलाई जाती थीं। इन दीपकों के लिए बड़ी मात्रा में घी की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए गाय, भेड़ और भैंस का पालन किया जाता था। शिलालेखों पर दिए गए सूक्ष्म विवरणों के अनुसार, घी का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक दीपक को आवंटित पशु संख्या या तो 96 भेड़े या 48 गाय या 16 भैंसे होती थीं। यह भी लिखा है कि राजराज के शासनकाल में, कुल 2,832 गायों, 1,644 भेडो और 30 भैंसों का चरवाहों द्वारा पालन किया जाता था, जिन्हें इसके लिए तंजावुर के पड़ोसी क्षेत्रों में ज़मीनें दी गईं थीं। इन चरवाहों का एकमात्र कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रतिदिन मंदिर में घी की आवश्यक मात्रा पहुँच जाए।

संध्याकाल में बृहदेश्वर मंदिर
राजराज ने स्पष्ट रूप से बृहदेश्वर मंदिर को एक ऐसे केंद्र में बदल दिया जहाँ कला और संस्कृति को महत्ता दी गई और वे समृद्ध हुईं। यह नृत्य का केंद्र बन गया और इसे वह स्थान कहा जाता है, जहाँ सादिर अट्टम (जिसे आज भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है) का जन्म हुआ। शिलालेखों के अनुसार राजराज ने चार सौ देवदासियों का संरक्षण किया, जो मंदिर की गतिविधियों से निकटता से जुड़ी थीं।
उन्होंने न केवल नर्तकियों का संरक्षण किया, बल्कि उन संगीतकारों का भी संरक्षण किया जो देवारम भजन गाते थे। कहा जाता है कि राजराज ने देवारम भजन गाने की लुप्त हो रही परंपरा को पुनर्जीवित किया। एक किंवदंती के अनुसार, राजराज चिदंबरम के नटराज मंदिर के एक कमरे में बंद, पत्तों पर उत्कीर्ण इन भजनों के समृद्ध खज़ाने को पाना चाहते थे। यह माना जाता था कि यह कमरा केवल तभी खोला जा सकता था जब सभी तमिल नयनार (संत) वहाँ उपस्थित हों। राजराज ने उनके नाम पर एक उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया और उनकी मूर्तियों को कमरे के सामने रख दिया। रहस्यमय तरीके से, ताला खुल गया और वे इन भजनों को प्राप्त करने में सफल रहे। इसलिए, राजराज को 'तमिल भजनों के रक्षक' के रूप में जाना जाता है। फिर उन्होंने संगीतज्ञों द्वारा तंजावुर में अपने मंदिर में इन भजनों के गाए जाने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने शिव (संभवत: चंद्रशेखर) की एक मूर्ती बनवाई, जिसके सामने रोज़ाना इन भजनों को गाया जाता था।

बृहदेश्वर मंदिर की कुछ मूर्तियाँ
नृत्य और संगीत ही नहीं, बल्कि बृहदेश्वर में चोल कला के कुछ और सर्वश्रेष्ठ निरूपण भी हैं। चोल कला शैली के अंतर्गत पत्थर और कांस्य की असाधारण मूर्तियाँ बनाई गईं। कुछ मूर्तियाँ दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। अपनी विस्तृत सूक्ष्मता और अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध, ये मूर्तियाँ भारतीय कला के समृद्ध संग्रह का हिस्सा हैं।
बृहदेश्वर मंदिर में, ये सुंदर मूर्तियाँ चारों दीवारों पर बनी हैं जो इस मंदिर की भव्यता को और बढ़ा देती हैं। भगवान शिव को समर्पित मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा हैं। विमान की पहली दो मंज़िलों में आले बने हैं जिनमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाती हुईं मूर्तियाँ बनी हैं।
इस महान मंदिर में, शिव की सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तियों में से एक नटराज है। चोल, नटराज (नृत्य के भगवान) के सबसे बड़े भक्त थे और यहाँ उन्हें चार भुजाओं के साथ अपनी विशिष्ट ब्रह्मांडीय मुद्रा में दर्शाया गया है, जिसमें उनका बायाँ पैर धड़ के ऊपर उठा हुआ है और दाहिना पैर अज्ञानता के दानव, अपस्मरा के ऊपर रखा हुआ है। ऊपरी बाएँ हाथ में अग्नि और ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है, जबकि निचले बाएँ हाथ को पैरों की ओर इशारा करते हुए शरीर के आगे और दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में दिखाया गया है।
शिव मूर्तियों के अलावा, द्वारपाल इस मंदिर की एक अन्य विशिष्टता हैं। बृहदेश्वर मंदिर के गर्भगृह के चार प्रवेश द्वारों और राजराजन गोपुरम की रक्षा करने वाली द्वारापाल की विशालकाय मूर्तियाँ, विशिष्ट चोल कला प्रदर्शित करती हैं।

नटराज की मूर्ति

बृहदेश्वर मंदिर के द्वारपाल
दिलचस्प रूप से, विमान की उत्तरी दीवार में एक सीधी रेखा में चार मानव आकृतियों की एक श्रृंखला बनी है। ये आकृतियाँ नीचे से ऊपर तक आकार में कम होती जाती हैं, और सबसे उपर की मूर्ती को टोपी पहने हुए दर्शाया गया है।
स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार, प्रभारी मूर्तिकार ने यहाँ पर तंजावुर के वर्तमान और भविष्य के शासकों की आकृतियों को बनाया था; एक चोल राजा की आकृति के साथ शुरू करते हुए, एक नायक, एक मराठा और अंत में एक यूरोपीय (टोपी वाली) आकृति बनाई गई थी। हालाँकि, यह तथ्य विवादित है। कई लोग मानते हैं कि यूरोपीय की आकृति को बाद में जोड़ा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि यह मूर्ती महान यात्री मार्को पोलो की है, जो शायद दक्षिण भारत आया होगा और उस समय का शासक पोलो की प्रसिद्धि से इस हद तक प्रभावित हुआ होगा कि उसने पोलो का चेहरा उस समय के सबसे बड़े विमान पर उत्कीर्णित करने का निर्णय लिया होगा।

विमान पर टोपी पहने एक मूर्ति
इस मंदिर के निर्माण में उपयुक्त प्रौद्योगिकी और वास्तु कौशल के अलावा, इसमें मौजूद विस्तृत शिलालेखों के कारण बृहदेश्वर एक असाधारण और अतुलनीय मंदिर बन गया है। कहा जाता है कि राजराज ने मंदिर के रख-रखाव से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी का अभिलेखन किया था। नियुक्त किए गए चौकीदारों की संख्या के विस्तृत विवरणों से लेकर, देवताओं के स्नान के पानी को सुगंधित करने के लिए कपूर खरीदने पर खर्च किए गए धन तक के विवरण, सभी, को मंदिर के शिलालेखों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है।
तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को देखकर आज भी आगंतुक अचंभित रह जाते हैं। यह तथ्य कि 1000 वर्षों के बाद भी 200 फ़ीट ऊँचा इस मंदिर विमान बिना किसी झुकाव के आज भी खड़ा है, यहाँ उपयुक्त अद्भुत वास्तु कौशल का प्रमाण है। यह मंदिर उन चोल मंदिरों में से एक है जिन्हें वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। वर्ष 2010 में, बृहदेश्वर ने अपने अस्तित्व के 1000 वर्ष पूर्ण किए और यह आज भी भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है।
 भारत सरकार
भारत सरकार


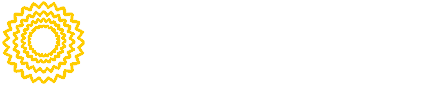 डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।
डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।
