ताजमहल
आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना एक विशाल मकबरा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहाँ ने 1631 से 1648 के बीच अपनी पसंदीदा बेगम की याद में बनवाया था। ताजमहल भारत में मुस्लिम कला का एक बेहतरीन नमूना है और इसे विश्व धरोहर की सर्वश्रेठ कलाकृतियों में से एक माना जाता है।
उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य
संक्षिप्त संश्लेषण
उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में यमुना नदी के दाएँ किनारे पर स्थित ताजमहल विशाल मुगल उद्यान का एक भाग है जो लगभग 17 हेक्टेयर के व्यापक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसे मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण-कार्य 1632 ईसवी में आरंभ हुआ था और 1648 ईसवी में यह मस्जिद, मेहमानख़ाने और दक्षिण के मुख्य प्रवेशद्वार के साथ बनकर तैयार हो गया था। बाहर के आँगन और उससे संबंधित तोरण-पथ का निर्माण-कार्य बाद में आरंभ हुआ जो 1653 ईसवी में बनकर तैयार हुए थे। इस इमारत पर अरबी लिपि में लिखे हुए अनेक ऐतिहासिक और कुरानी अभिलेख मौजूद हैं जिनके आधार पर ताजमहल के कालानुक्रम को निर्धारित किया जा सकता है। इसके निर्माण-कार्य के लिए मुगल साम्राज्य तथा मध्य एशिया और ईरान से राजगीरों, संगतराशों, कोफ़्तगारों, नक्काशीकारों और अन्य कारीगरों को काम पर लगाया गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुशिल्पकार थे।
ताजमहल को वास्तुकला की दृष्टि से समस्त भारतीय-इस्लामी संरचनाओं में एक सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना जाता है। इसकी बेहतरीन वास्तुकला में घनपन और रिक्तता का, अवतलता और उत्तलता का, धूप और छाँव का लयबद्ध मेल-मिलाप है। मेहराब और गुंबद इसकी सुंदरता में चार चाँद लगाते हैं। प्रकृति की हरियाली, वीथिका के लाल-भूरेपन और इसके ऊपर फैले हुए आसमान के नीलेपन की युति के कारण यह स्मारक प्रकृति के हर तरह के रूप और माहौल में देखते ही बनता है। संगमरमर पर की गई नक्काशी और उसमें जड़े हुए कीमती और अर्ध कीमती रत्न इस स्मारक को अनोखा बना देते हैं।
ताजमहल के अनूठेपन का कारण शाहजहाँ के उद्यान विशेषज्ञों और वास्तुशिल्पकारों के कार्यों में पाई जाने वाली विलक्षण नवीनता है। मकबरे को चौतरफ़े उद्यान के बीचों-बीच स्थापित करने के बजाय उसे उद्यान के एक छोर पर स्थापित करना ऐसी ही एक श्रेष्ठ योजना है जिसके कारण इस मकबरे को दूर से देखने पर भी एक त्रिआयामी दृश्य दिखाई देता है। इसके अलावा, यह ज़मीन से उठे हुए मकबरों की किस्म का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह मकबरा, जिसे एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाया गया है, उसकी मीनारों के अष्टभुजाकार तल के चार किनारें, कोनों पर स्थित वर्ग से बाहर की ओर निकलते हैं। चबूतरे के ऊपरी भाग पर दक्षिणी किनारे के मध्य में मौजूद सीढ़ियों से पहुँचा जा सकता है। ताजमहल का ज़मीनी नक़्शा इस संरचना का सटीक संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। संरचना के मध्य में अष्टभुजाकार समाधि कक्ष है जो प्रवेशकक्षों और चार कोनों में बने कमरों से घिरा हुआ है। ऊपरी मंज़िल पर यही योजना दोहराई गई है। मकबरे के बाह्य भाग की योजना वर्गाकार है जिसके सममित ढलान वाले कोनें हैं। भव्य दुमंज़िला गुंबदीय कक्ष जिसमें मुमताज़ महल तथा शाहजहाँ की कब्रें हैं, उसकी योजना अष्टभुजाकार है। दोनों कब्रें चारों ओर से जिस नक्काशीदार जाली से घिरी हुईं हैं, वह कारीगरी का एक उत्कृष्ट नमूना। यह जाली अत्यधिक चमकदार है और उत्कृष्ट जड़ाई के काम से सजी हुई है। चौखटों के किनारों पर फूलों के आकार में रत्नों को उत्कृष्ट ढंग से जड़ा गया है। पत्ते और फूल बनाने के लिए रत्नों के जिन रंगों और रंगतों का उपयोग किया गया है, उसके कारण वे असली लगते हैं। मुमताज़ महल की कब्र समाधि कक्ष के बिल्कुल मध्य में एक आयाताकार चबूतरे पर स्थित है जिसपर फूल के पौधों के रूपांकनों को जड़ाई के काम से अलंकृत किया गया है। शाहजहाँ की कब्र मुमताज़ महल की कब्र से बड़ी है जिसे लगभग तीस साल बाद मुमताज़ महल की कब्र की पश्चिमी ओर बनाया गया था। यहाँ दिखाई देने वाली कब्रें नकली हैं; असली कब्रें निचले समाधि कक्ष (शवखाना) में हैं। कब्रें बनाने की यह पद्धति जो शाही मुगल मकबरों में अपनाई गई थी।
चबूतरे के कोनों पर स्वतंत्र रूप से खड़ीं चार मीनारें मुगल वास्तुकला को एक अलग ही गहराई प्रदान करती हैं। इन चार मीनारों के कारण इस स्मारक को न केवल एक स्थानिक संदर्भ मिलता है, बल्कि ये इस इमारत को एक त्रिआयामी रूप भी प्रदान करती हैं।
ताजमहल के परिसर में सबसे अधिक प्रभावशाली संरचना मकबरे के बगल में स्थित मुख्य दरवाज़ा है जो सामने के आँगन की दक्षिणी दीवार के मध्य में बड़ी शान से खड़ा है। दरवाज़े के उत्तरी भाग की दोनों ओर एक-एक गलियारा है। गलियारों के सामने बना हुआ उद्यान दो मुख्य रास्तों द्वारा चार भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग फिर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले, सँकरे रास्तों द्वारा विभाजित हैं। यह रचना तैमूरी-फ़ारसी शैली में दीवारों से घिरे हुए उद्यान के आधार पर बनाई गई है। पूर्व और पश्चिम की बाहरी दीवारें जहाँ मिलती हैं, वहाँ मध्य में एक मंडप है।
ताजमहल योजनाबद्ध तरीक़े से बनवाई गई एक बेहतरीन सममितीय इमारत है। द्विपक्षीय सममिति से युक्त इसके केंद्रीय अक्ष पर मुख्य संरचनाएँ स्थित हैं। इसके निर्माण में ईंट और चूने के गारे का उपयोग किया गया है जिस पर लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का मुलम्मा चढ़ाया गया है और किमती और अर्ध कीमती रत्नों का जड़ाई का काम किया गया है। ताजमहल के परिसर के मध्य में संगमरमर से बने मकबरे के विपरीत मस्जिद और मेहमानखाना लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। दोनों इमारतों की छत पर सामने की ओर एक बड़ा चबूतरा है। दोनों संरचमाएँ दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। उनमें एक भव्य आयताकार इबादतखाना है जिसमें एक पंक्ति में तीन मेहराबदार कक्ष हैं और मध्य में एक बड़ा प्रवेशकक्ष है। प्रवेशकक्ष की मेहराबों की चौखट और मेहराब के शिखर तथा आयताकार चौखट के बीच दिखाई देने वाले लगभग त्रिभुजाकार स्थानों (स्पांड्रिल) पर सफ़ेद संगमरमर का मुलम्मा चढ़ाया गया है। ये त्रिभुजाकार स्थान स्टोन इंटार्सिया के फूलदार अरबस्कों से भरे हुए हैं और मेहराबों के किनारे रस्सीनुमा पट्टी से सजाए गए हैं।
मापदंड(1)- ताजमहल में उत्तम सामंजस्य और उत्कृष्ट कारीगरी होने के कारण यह भारतीय-इस्लामी पद्धति के मकबरों की संपूर्ण शृंखला में वास्तुकला और कलात्मकता की दृष्टि से एक बेहतरीन संरचना है। यह संकल्पना, निरूपण और निष्पादन की दृष्टि से एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है और इसके अनूठे सौंदर्यपरक तत्वों में संतुलन और सममिति है तथा विभिन्न तत्वों का सामंजस्यपूर्ण मेल है।
समग्रता
मकबरे, मस्जिद, मेहमानखाने, मुख्य दरवाज़े और पूरे ताजमहल परिसर की अक्षुण्णता द्वारा यहाँ की समग्रता स्थापित होती है। ताजमहल का बाहरी रूप अच्छी स्थिति में है। इस संरचना की स्थिरता, इसकी नींव का स्वरूप, मीनारों का खड़ापन और निर्माण संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन किया गया है और इनकी देखरेख लगातार जारी है। प्रदूषण से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए हवा की गुणवत्ता को लगातार मापने हेतु और क्षय कारकों के पैदा होते ही उन्हें नष्ट करने हेतु वायु प्रदूषण मापक यंत्र लगाया गया है। इस परिवेश की सुरक्षा को सुनिशचित करने के लिए विस्तारित बफ़र ज़ोन में योग्य प्रबंधन और विनियमों को लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही, भविष्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए विकास-कार्यों को चलाते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि, आगरा के किले सहित, इस क्षेत्र की कार्यात्मक और दृश्यात्मक अखंडता बनी रहे।
प्रामाणिकता
मकबरा, मस्जिद, मेहमानखाना, मुख्य दरवाज़ा और वैसे देखा जाए, तो पूरे ताजमहल परिसर की ही प्रामाणिकता वैसी ही बनी हुई है जैसी इसके अभिलेखन के समय थी। हालाँकि अंग्रेज़ी शासनकाल से ही बड़ी मात्रा में मरम्मत तथा संरक्षण के कार्य चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनके कारण इन इमारतों की मूल विशेषताओं पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। भविष्य में चलाए जाने वाले संरक्षण-कार्यों के लिए ऐसे निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इमारतों के आकार और रूप जैसी विशेषताएँ संरक्षित बनी रहें।
सुरक्षा तथा प्रबंधन संबंधी आवश्यकताएँ
ताजमहल परिसर का प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। इस स्मारक की कानूनन सुरक्षा और इसके आसपास के विनियमित क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विविध वैधानिक और विनियामक रूपरेखाएँ स्थापित की गईं जिनमें प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, और नियम 1959, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और प्रमाणीकरण) शामिल हैं, जो इस क्षेत्र और बफ़र क्षेत्रों के समग्र प्रशासन के लिए पर्याप्त हैं। अन्य सहायक कानून, इस क्षेत्र के आस-पास होने वाले विकास-कार्यों के संदर्भ में, इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए इस स्मारक के आसपास का 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। दिसंबर 1996 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय लिया
जिसके अनुसार ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीज़ेड) में स्थित उद्योगों में कोयले/कोक के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया और उन उद्योगों को या तो प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने को या फिर टीटीज़ेड से बाहर स्थानांतरित होने का निर्देश दिया। टीटीज़ेड में 40 संरक्षित स्मारकों का समावेश है जिनमें से तीन विश्व धरोहर स्थल हैं - ताजमहल, आगरे का किला और फ़तेहपुर सीकरी।
केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि बफ़र क्षेत्रों के लिए पर्याप्त है। इस परिसर में संपूर्ण संरक्षण, परिरक्षण तथा रखरखाव की गतिविधियाँ चलाने के लिए तथा आगरा सर्किल के अधीक्षक पुरातत्ववेत्ता के नेतृत्व में इन गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए भी यह धनराशि पर्याप्त है। यहाँ की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन आवश्यक है, विशेषकर इस क्षेत्र में पर्यटन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले दबाव के परिप्रेक्ष्य में, जिसके यथोचित प्रबंधन की भी आवश्यकता है। प्रबंधन योजना में अवसंरचना के प्रस्तावित विकास-कार्यों के लिए भी यथोचित दिशानिर्देश होने चाहिए और साथ में, एक व्यापक सार्वजनिक उपयोग की योजना स्थापित की जानी चाहिए।
ताजमहल (जिसका नाम शुरू में रौज़ा-ए-मुनव्वरा, यानी ‘एक चमकता हुआ मकबरा’ था) मुगल वास्तुकला की श्रेणी का सबसे बेहतरीन नमूना है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने 1632 में अपनी मरहूम बेगम मुमताज़ महल के मकबरे के रूप में करवाया था। ताजमहल, एक आला दर्जे के सरदार से खरीदी गई ज़मीन पर बनवाया गया था। यह भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इस स्मारक की योजना तथा निर्माण की ज़िम्मेदारी वास्तुशिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी तथा मीर अब्दुल करीम को सौंपी गई थी। मकरामत खान व्यवस्थापन का काम देखते थे। ताजमहल दुनियाभर में अमर प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस मकबरे को वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया।
शहज़ादा खुर्रम (जो बाद में शाहजहाँ कहलाए गए) अपने वालिद जहाँगीर के बाद बादशाह बने। उन्होंने तीस साल (शासनकाल 1628-1658) शासन किया। शाहजहाँ और अर्जुमंद बानो बेगम का निकाह उनकी सगाई के पाँच साल बाद हुआ। अर्जुमंद को बाद में मुमताज़ महल नाम दिया गया। मुमताज़ महल हर वक्त बादशाह के साथ रहने लगीं और, 1631 में अपनी मृत्यु तक, शाहजहाँ की सभी लशकरी मुहिमों में उनके साथ जाती रहीं। बेगम की मृत्यु बुरहानपुर में होने के कारण उन्हें वहीं पर एक उद्यान में कुछ समय के लिए दफ़नाया गया था; छह महीने बाद उनके शव को आगरा ले जाकर उसे एक ऐसे स्थल पर दफ़नाया गया था जिसे उनके मकबरे के निर्माण के लिए चुना गया था। शाहजहाँ अपनी बीवी के बाद एक लंबे अरसे तक जीवित रहे और 1666 में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उनके जीवन के आखिरी आठ साल शाही दरबार की सुख-सुविधओं में नहीं बीते। उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें आगरे के किले में कैद कर लिया था जहाँ उनका जीवन एकदम एकाकी बीता। इस किले से ताजमहल दिखाई देता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को ताजमहल में ही मुमताज़ महल के बगल में दफ़नाया गया।
मकबरे के उद्यान के दो भाग हैं : चार बाग की शैली में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले रास्तों से युक्त उद्यान और एक चबूतरा जिस पर यह मकबरा स्थित है। मकबरे की शैली फ़ारसी-सफ़वी गुंबदों से तथा उस्मानी और भारतीय वास्तुकला के तत्वों से प्रभावित है। यह मकबरा, समरकंद में स्थित गोर-ए-अमीर नामक तैमूर के मकबरे तथा दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद जैसी तैमूरी और मुगल इमारतों से भी प्रभावित है। खास अंतर बस यही है कि पहले की मुगल इमारतें लाल बलुआ पत्थर से बनवाई गई थीं जबकि ताजमहल पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर और अर्ध कीमती रत्नों से बनवाया गया है।
इस परिसर का मुख्य आकर्षण वह मकबरा है जिसमें शाहजहाँ तथा मुमताज़ महल की कब्रें हैं। ये कब्रें बारीकी से तराशी गई संगमरमर की जाली से घिरी हुई हैं। इस जाली की सतह पर फलों, फूलों और बेलों की सुंदर नक्काशियाँ हैं। प्रत्येक शवपेटिका पर कीमती और अर्ध कीमती रत्न जड़े हैं और साथ-ही-साथ इन पर कैलिग्राफ़ीयुक्त अभिलेख भी हैं।
आंतरिक गुंबद के ऊपर बाहरी गुंबद बना हुआ है जिसके प्रत्येक कोने पर एक-एक छोटी छतरी बनी हुई है। परिसर तीन तरफ़ से लाल बलुआ पत्थर से बनीं दीवारों से घिरा हुआ है; केवल नदी की ओर का भाग खुला छोड़ दिया गया है। अन्य सभी आयताकार मुगल उद्यानों के विपरीत, जिनके मध्य में मकबरा स्थित होता है, ताजमहल का उद्यान मकबरे को चारों ओर से घेरने के बजाय मकबरे के सामने बना है।

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara

© E. de Gracia Camara
Author: E. de Gracia Camara
 भारत सरकार
भारत सरकार


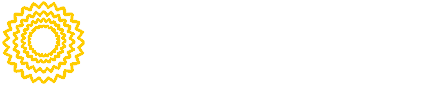 डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।
डिजिटल भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, ‘भारतीय संस्कृति’ पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक पहल है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो पूरे भारत की विभिन्न रिपॉज़िटरियों और संस्थानों से सांस्कृतिक प्रासंगिकता के डेटा को प्रस्तुत करता है।
